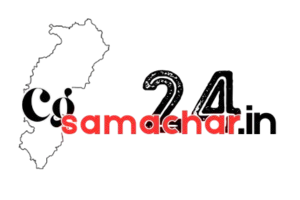दीवारों के पार की आवाज – आईये जानते हैं एक पत्रकार कुमार जितेन्द्र की जेल डायरी…..
CG Samachar 24.in
संपादकीय :- दीपक गुप्ता….✍️
पत्रकार कुमार जितेंद्र के कलम से….✍️
अध्याय 1: वह दिन जब खबर, खुद खबर बन गई
वर्ष 2009 — मैं उस दिन ग्राम पंचायत के कुछ खामियों को लेकर एक खबर तैयार करने गया था।
वहाँ घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें थीं। मैं पत्रकार के नाते सच्चाई उजागर करने पहुँचा — पर जल्द ही सबकुछ उल्टा हो गया।
सरपंच ने मुझे धमकाया और पुलिस से कह दिया —
“यह अवैध वसूली करने आया है।”
आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ के कुछ स्थानीय पत्रकार भी इस षड्यंत्र में शामिल थे।
देखते ही देखते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा लिखा-पढ़ी दो घंटे में जैसे पहले से तैयार थी — एफआईआर, गवाह, बयान… सब कुछ।
मुझे थाने से सीधे न्यायालय ले जाया गया — लेकिन वहाँ मेरी कोई बात नहीं सुनी गई।
ना जमानत, ना दलील — सीधा आदेश – न्यायिक अभिरक्षा।
मुझे जेल भेज दिया गया।
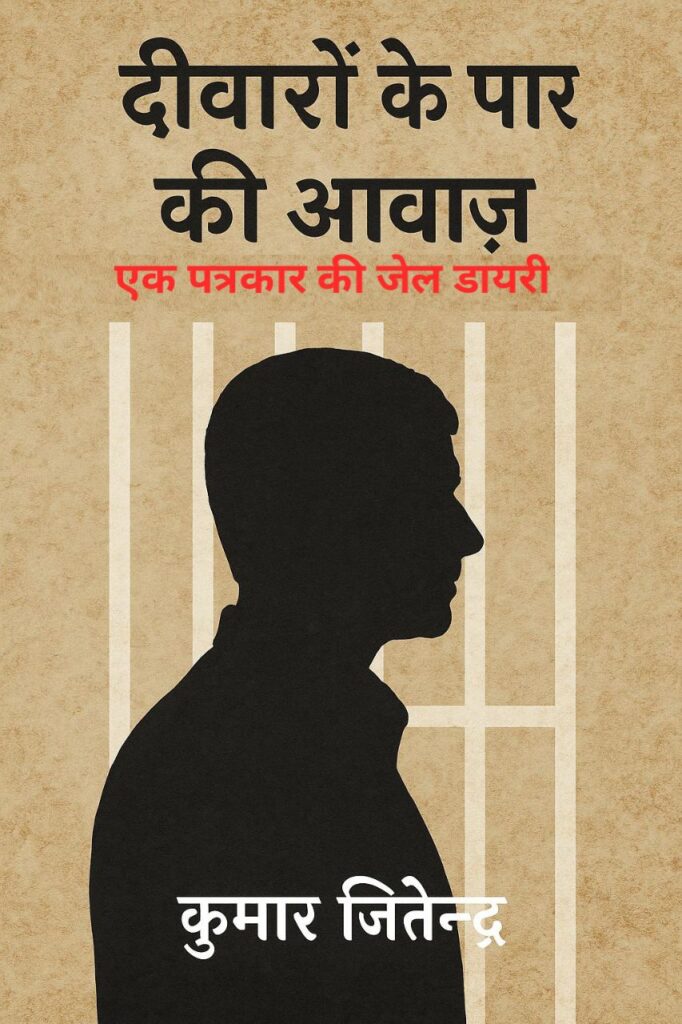
अध्याय 2: सलाखों की सच्चाई :- जेल में पहली बार कदम रखा। दिल थरथरा रहा था।
चारों तरफ़ मुझे घूरती निगाहें थीं — हत्यारे, नक्सली, बलात्कारी, चोर और डकैत।
मैं एक कोने में सहमा खड़ा था।
एक नक्सली ने पूछा —
“किस केस में आए हो?”
मैं डरते हुए बोला —
“पत्रकार हूँ, सड़क की खराबी पर रिपोर्ट की थी…”
वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला —
“अरे! पत्रकार हो? आओ, मेरे बगल में सो जाओ।”
वो पहली राहत थी — सम्मान की एक झलक, उस जगह पर जहाँ उम्मीदें मर जाया करती हैं।
अगली सुबह शुरू हुई — सीटी की आवाज से।
गिनती, खाना, शौचालय — कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बैरक के नियम-कायदों की अपनी दुनिया थी।
पर मुझे तो बस एक बात सता रही थी —
“मैं यहाँ से कब बाहर निकलूँगा?”
जेल अधिकारियों का रवैया सामान्य था — न कठोर, न खास सहयोगी।
इसी बीच मैंने पहली बार सुना —
“भाई, हम तो निर्दोष हैं… बीवी ने केस कर दिया… पैसे नहीं थे वकील करने को।”
मैं चौंका। फिर एक ने कहा —
“घर का झगड़ा था… अब डेढ़ साल से यहीं पड़े हैं।”
धीरे-धीरे समझ आया —
यहाँ ज्यादातर लोग अपराधी नहीं, मजबूर हैं।
सिस्टम की खामियों ने उन्हें अपराधी बना दिया।
एक दिन एक जेल अधिकारी मुझे गौर से देखने लगा।
फिर उसने एक बंदी से कहा
“इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पत्रकार हैं।”
वो पल मेरे लिए दोहरी अनुभूति वाला था —
एक तरफ पहचान की राहत थी, दूसरी तरफ डर,
कि कहीं ये पहचान खतरा न बन जाए।
लेकिन उसी पहचान ने मुझे धीरे-धीरे वहाँ सम्मान दिलाया।
अब कैदी अपने केस के दस्तावेज लेकर मेरे पास आने लगे।
मैं कोई वकील नहीं था — बस उनकी बात सुन सकता था।
और यही सबसे बड़ी राहत बन गई —
मैंने रोज उनकी बातें सुनना शुरू किया।
उनमें से कुछ लोग मुझे सुबह से इंतजार करते थे —
सिर्फ ये पूछने कि “आपको लगता है मैं छूट जाऊँगा?”
दसवें दिन, मुझे सशर्त जमानत मिल गई।
जब बाहर निकला, तो जेल के फाटक पर मुड़कर देखा
उन कैदियों की आँखें अब मुझे ‘पत्रकार’ नहीं,
एक ‘सुनने वाला इंसान’ समझ रही थीं।
ठीक पाँच वर्ष बाद सन 2014 में सच सामने आ गया और मैं उस मामले में दोष मुक्त हो गया। इसीलिए कहा गया है कि सच को पराजित नहीं किया जा सकता।